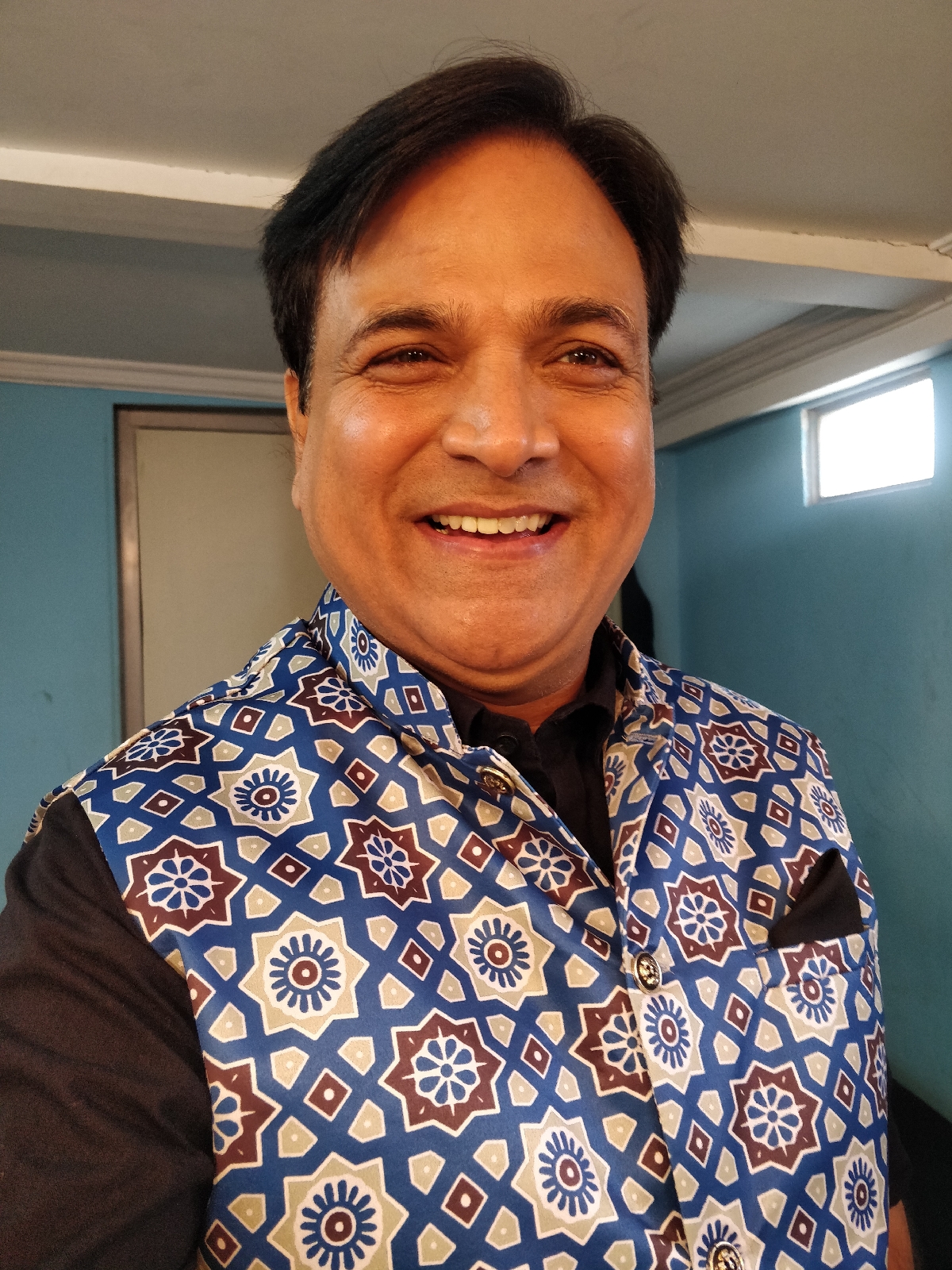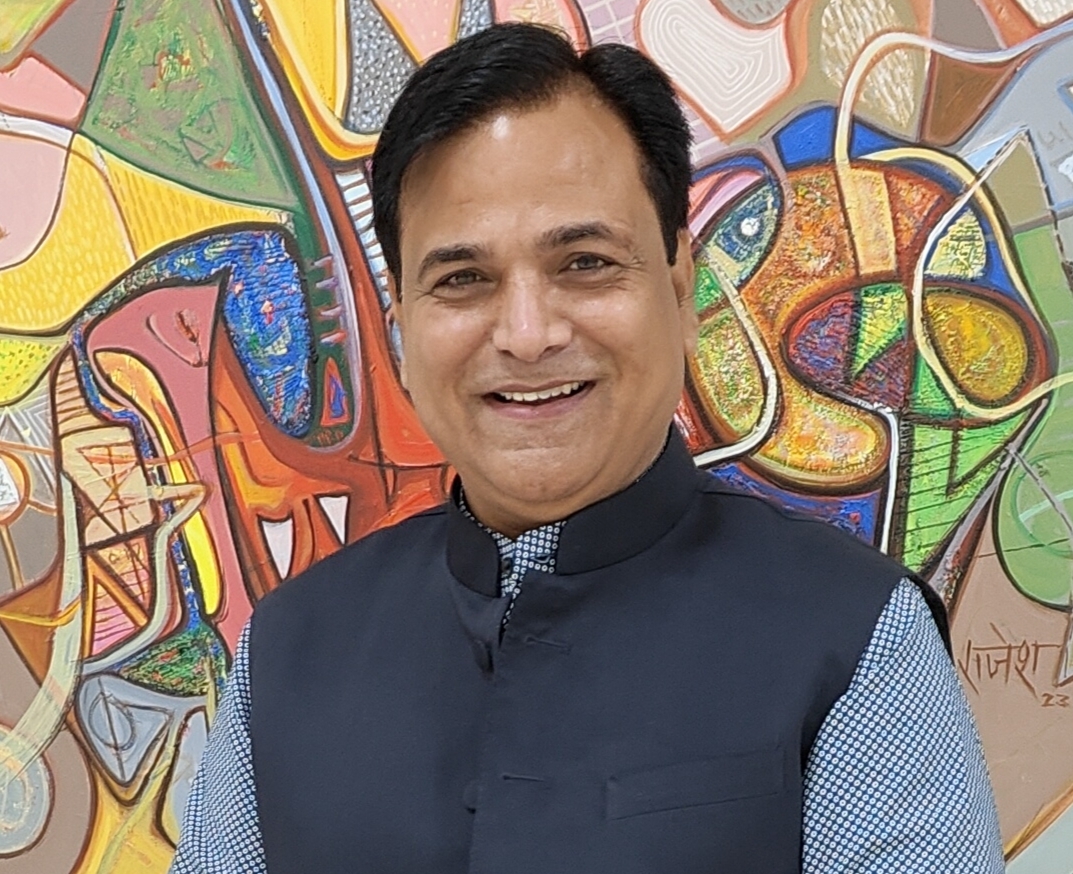रस और उनका क्रम

जानें... जीवन के 'रस' और उसके 'क्रम' को 'अष्टौ नाट्ये रसा: स्मृता:' भरत मुनि ने आठ रसों का ही उल्लेख किया है । इसी के आधार पर महाकवि कालिदास भारवि और दंडी ने भी इन्ही 8 रसों का ही प्रतिपादन किया है । भरत मुनि ने इन रसों का क्रम भी निर्धारित किया है, १. शृङ्गार, २. हास्य, ३. करुण, ४. रौद्र, ५ वीर, ६. भयानक, ७. बीभत्स और ८. अद्भुत-नाटक में ये आठ ही रस माने जाते हैं । रति या काम न केवल मनुष्य जाति में अपितु सभी जातियों में मुख्य प्रवृत्तिके रूप में पाया जाता है और सबको उसके प्रति आकर्षण होता है, इसलिए सबसे पहले शृङ्गार को स्थान दिया गया है। हास्य शृङ्गार का अनुगामी है, इसलिए शृङ्गार के बाद हास्यरस को स्थान दिया गया है। हास्य से विपरीत स्थिति करुणरस की है। इसलिए हास्यके बाद करुणरस को स्थान दिया गया है। अपने प्रियतम बन्धुके वास्तविक विनाश या भ्रमवश ही उसके विनाश का निश्चय हो जाने के बाद करुणरस की सीमा प्रारम्भ होती है, उसमें पुनर्मिलनकी आशा नहीं रहती है। अतएव करुणरस नैराश्यमय होनेसे निरपेक्ष-रस माना जाता है। भवभूतिने 'तटस्थं नैराश्यात्' कहकर करु